Table of Contents
संधि की परिभाषा और उसके भेद तथा उदाहरण – हिंदी व्याकरण
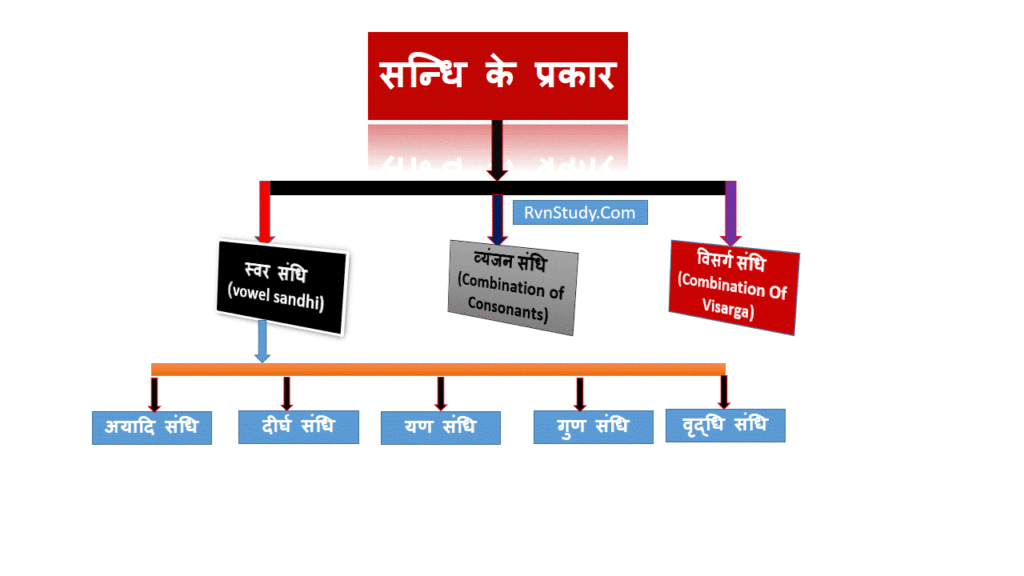
संधि की परिभाषा लिखिए –
परिभाषा – दो वर्णो के आपस मे मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है अथवा दो वर्णों ध्वनियों) के मिलने से जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते है।
जैसे :- सती + ईश = सतीश
परिभाषा – दो वर्णो के आपस मे मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है अथवा दो वर्णों ध्वनियों) के मिलने से जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते है।
जैसे :- सती + ईश = सतीश
मनः + योग = मनोयोग
सत + जन = सज्जन
मनः + योग = मनोयोग
संधि के प्रकार (Sandhi ke Bhed)-
संधि के भेद – संधि 3 प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित है –
- स्वर संधि
- व्यंजन संधि
- विसर्ग संधि
(I) स्वर संधि किसे कहते है –
परिभाषा – जब दो स्वरों का आपस मे एक दूसरे से मिलन होता है अर्थात एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है, अथवा दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं।
जैसे – हिम् + आलय = हिमालय
सत्य + आग्रह = सत्याग्रह
महा + आशय = महाशय
गर्व + आधान = गर्भाधान
स्वर संधि कितने प्रकार होती है –
स्वर संधि 5 प्रकार की होती है.
- – दीर्घ स्वर संधि
- – गुण स्वर संधि
- – वृध्दि स्वर संधि
- – यण स्वर संधि
- – अयादि स्वर संधि
1. दीर्घ संधि किसे कहते है –
परिभाषा – जब दीर्घ या ह्रस्व स्वर (‘अ’ ‘इ’ ‘उ’) के बाद समान दीर्घ या ह्रस्व स्वर (‘अ’ ‘इ’ ‘उ’) आएँ तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर (‘आ’ ‘ई’ ‘ऊ’) हो जाते है, अथवा हस्व स्वर (अ,इ,उ) या दीर्घ स्वर (आ, ई,ऊ) के आपस में मिलने से यदि स्वर्ण या उसी जाति के दीर्घ स्वर (आ,ई, ऊ) की उत्पत्ति हो, तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं।
दीर्घ स्वर संधि को बनाने और पहचाने का तरीका – दीर्घ संधि की पहचान – दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशत आ, ई, ऊ की मात्राएँ ( ा, ी ू) आती है और इनका विच्छेद इन्ही मात्राओं से किया जाता है|
| दीर्घ संधि बनाना/पहचानना | संधि विच्छेद |
|---|---|
| अ + अ = आ | पुस्तक + अर्थी = पुस्तकार्थी कल्प + अंत = कल्पांत मत + अनुसार = मतानुसार गीत + अंजलि = गीतांजलि परम + अर्थ = परमार्थ स्व + अर्थी = स्वार्थी धर्म + अर्थ = धर्मार्थ नयन + अभिराम = नयनाभिराम |
| अ + आ = आ | भय + आकुल = भयाकुल सत्य + आग्रह = सत्याग्रह देव + आलय = देवालय नव + आगत = नवागत रत्न + आकर = रत्नाकर कुश + आसन = कुशासन जल + आगम = जलागम परम + आत्मा = परमात्मा स्वर + आदेश = स्वरादेश स्व + आनंद = स्वानंद ब्रम्हचर्य + आश्रम = ब्रम्हाचर्याश्रम आयुध + आगार = आयुधागार वज्र + आयुध = वज्रायुध हत + आश = हताश |
| आ + अ = आ | सेवा + अर्थ = सेवार्थ तथा + अपि = तथापि कदा + अपि = कदापि परीक्षा + अर्थी = परीक्षार्थी सीमा + अंत = सीमान्त रेखा + अंश = रेखांश पूरा + अवशेष = पुरावशेष विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास |
| आ + आ = आ | प्रेक्षा + आगार = प्रेक्षागार वार्ता + आलाप = वार्तालाप विद्या + आलय = विद्यालय महा + आशय = महाशय महा + आत्मा = महात्मा रचना + आत्मक = रचनात्मक |
| इ + इ = ई | रवि + इंद्र = रवींद्र कवि + इन्द्र = कवीन्द्र मुनि + इन्द्र = मुनीन््द्र अति + इत = अतीत गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्र |
| इ + ई = ई | हरि + ईश = हरीश गिरि + ईश = गिरीश परि + ईक्षक = परीक्षक अधि + ईश्व = अधीश्वर मुनि + ईश्व = मुनीश्वर कपि + ईश = कपीश क्षिति + इश = क्षितीश |
| ई + इ = ई | फणी + इन्द्र = फणीन्द्र यती + इन्द्र = यतीन्द्र महती + इच्छा = महतीच्छा देवी + इच्छा = देवीच्छा नारी + इच्छा = नारीच्छा |
| ई + ई = ई | मही + ईश = महीश नदी + ईश्वर = नदीश्वर रजनी + ईश = रजनीश सती + ईश = सतीश फणी + ईश्वर = फणीश्वर |
| उ + उ = ऊ | भानु + उदय = भानूदय सु+ उक्ति = सूक्ति लघु + उत्तम = लघूत्तम अनु + उदित = अनूदित विधु + उदय = विधूदय |
| उ + ऊ =ऊ | अंबु + ऊर्मि = अम्बुर्मि लघु + ऊर्मि = लघूर्मि सिंघु + ऊर्मि = सिंधूर्मि |
| ऊ + उ = ऊ | वधू + उत्सव = वधूत्सव भू + उत्सर्ग = भूत्सर्ग चमू + उत्साह = चमूत्साह वधू + उल्लास = वधूल्लास भू + उपरि = भूपरि |
| ऊ + ऊ =ऊ | भू+ ऊर्जा = भूर्जा सरयू + ऊर्मि = सरयूर्मि भू+ ऊषर = भूषर |
दीर्घ संधि के उदाहरण –
मध्य + अवधि = मध्यावधि
कर + अधिकारी = कराधिकारी
परम + अर्थ = परमार्थ
देश + अंतर = देशांतर
दिवस + अवसान = दिवसावसान
दीप + अवली = दीपावली
चन्द्र + अस्त = चन्द्रास्त
मूल्य + अंकन = मूल्यांकन
बीज + अंकुर = बीजांकुर
नयन + अंबु = नयनांबु
नव + अंकुर = नवांकुर
जठर + अग्नि = जठराग्नि
काम + अयनी= कामायनी
विष + अणु = विषाणु
परम + अणु = परमाणु
दिव्य + अस्त्र = दिव्यास्त्र
रोम + अवली = रोमावली
धर्म + अधर्म = धर्माधर्म
रत्न + अवली = रत्नावली
पंच + अमृत = पंचामृत
अक्ष + अंश = अक्षांश
निम्न + अनुसार = निम्नानुसार
मोह + अंध = मोहान्ध
नर + अधिप = नराधिप
चरण + अमृत = चरणामृत
पंच + अग्नि = पंचाग्नि
स्व + अर्थ = स्वार्थ
पद + अधिकारी = पदाधिकारी
प्रसंग + अनुकूल = प्रसंगानुकूल
पाठ + अंतर = पाठांतर
सूर्य + अस्त = सूर्यास्त
नील + अंबर = नीलांबर
उप + अध्यक्ष = उपाध्यक्ष
भाव + अंतर = भावान्तर
देह + अतीत = देहातीत
बल + अध्यक्ष = बलाध्यक्ष
कीट + अणु = कीटाणु
ब्रह्म + अस्त्र = ब्रह्मास्त्र
पूर्ण + अंक = पूर्णाक
यक्ष + अधिपति = यक्षाधिपति
तीर्थ + अटन = तीर्थाटन
लोक + अधिपति = लोकाधिपति
राज्य + अभिषेक = राज्याभषिक
शब्द + अलंकार = शब्दांकार
वेद + अंत = वेदांत
विकल + अंग = विकलांग
मुख + अग्नि = मुखाग्नि
वेद + अलंकार = वेदालंकार
वीर + अंगना = वीरांगना
सत्य + असत्य = सत्यासत्य
हिम + अंचल = हिमाचल
क्षार + अक्ष = क्षाराक्ष
समान + अधिकार = समानाधिकार
स + अवधान = सावधान
हरिण + अक्षी = हरिणाक्षी
स्व + अवलंबी = स्वावलंबी
दीर्घ संधि में अपवाद शब्द
दीर्घ संधि में अपवाद शब्द – दीर्घ संधि में कुछ ऐसे शब्द भी है जो दी गई परिभाषा या नियम को फॉलो नहीं करते है फिर भी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते है इसलिए ऐसे शब्दों हमेशा यद् रहना चाहिए क्युकी इस प्रकार के शब्द अपवाद स्वरुप परीक्षाओं में पूछे जाते है. जिससे छात्रो को संधि पहचानने में थोड़ी समस्या होती है. दीर्घ संधि के ऐसे शब्दों की सूची निम्नलिखित है –
शक + अंधु = शकन्धु
पितृ + ऋण = पितृण
विश्व + मित्र = विश्वामित्र
कर्क + अंधु = कर्कन्धु
मूसल + धार = मूसलाधार
युवन + अवस्था = युवावस्था
मनस + ईषा = मनीषा
2. गुण संधि किसे कहते है
जब अ तथा आ के बाद ‘इ’ या ‘ई’, ‘उ’ या ‘ऊ’ और ‘ऋ’ स्वर आये तो दोनों स्वर मिलकर ‘ए’, ‘ओ‘ और ‘अर’ हो जाते है, तब वहाँ गुण स्वर संधि होती है|
गुण संधि के उदाहरण –
| गुण संधि | संधि विच्छेद |
|---|---|
| अ + इ = ए | गज + इन्द्र = गजेन्द्र भारत + इन्द्र = भारतेन्द्र न+ इति = नेति जित + इन्द्रिय = जितेन्द्रिय मृग + इन्द्र = मृगेन्द्र |
| आ + इ = ए | महा + इन्द्र = महेंद्र यथा + इष्ट = यथेष्ट राजा + इन्द्र = राजेन्द्र रसना + इन्द्रिय = रसनेन्द्रिय |
| अ + ई = ए | कमल + ईश = कमलेश परम + ईश्वर = परमेश्वर राज + ईश = राजेश योग + ईश्वर = योगेश्वर उप + ईक्षा = उपेक्षा नर + ईश = नरेश सर्व + ईश्वर = सर्वेश्वर |
| आ + ई = ए | लंका + ईश = लंकेश रमा + ईश = रमेश राका + ईश = राकेश महा + ईश = महेश महा + ईश्वर = महेश्वर |
| अ + उ = ओ | वीर + उचित = वीरोचित रोग + उपचार = रोगोपचार सूर्य + उदय = सूर्योदय चन्द्र + उदय = चंद्रोदय मद + उन्माद = मदोन्माद अंत्य + उदय = अंत्योदय |
| अ + ऊ = ओ | नव + ऊढ़ा = नवोढ़ा सूर्य + ऊष्मा = सूर्योष्मा समुद्र + ऊर्मि = समुद्रोर्मि जल + ऊर्मि = जलोर्मि |
| आ + उ = ओ | महा + उत्सव = महोत्सव यथा + उचित = यथोचित महा + उदधि = महोदधि महा + उदय = महोदय करूणा + उत्पादक = करूणोत्पादक |
| आ + ऊ = ओ | महा + ऊर्जा = महोर्जा गंगा + ऊर्मि = गंगोर्मी महा + उदधि = महोदधि यमुना + ऊर्मि = यमुनोर्मि |
| अ + ऋ = अर | देव + ऋषि = देवर्षि सप्त + ऋषि = सप्तर्षि शीत + ऋतु = शीतर्तु ब्रह्म + ऋषि = ब्रह्मर्षि |
| आ + ऋ = अर | महा + ऋषि = महर्षि |
3. वृद्धि संधि किसे कहते है
जब अ’ या आ’ स्वर के बाद ‘ए* या ‘ऐ’ स्वर आते हैं तो ‘ऐ” बनता और अ’ या “आ’ स्वर के बाद “ओ’ या औ’* स्वर आने पर “औ’ हो जाता है। ‘ऐ” व ‘औ’ दोनों वृद्धि स्वर होने के कारण यह संधि वृद्धि संधि कहलाती हैं.
वृद्धि संधि के उदाहरण –
| अ/आ+ए/ऐ = ऐ | एक+एक = एकैक सदा+एव = सदैव तथा+एव = तथैव मत+एक्य = मतैक्य गंगा+ऐश्वर्य = गंगैश्वर्य |
| अ+ओ = औ | |
| आ+ओ = औ | |
| अ+औ = औ | |
| आ +औ = औ |
4. यण संधि किसे कहते है
यण संधि के नियम- यदि ’इ’, ‘ई’, ‘उ’, ‘ऊ’ और ‘ऋ’के बाद कोई भित्र स्वर आये, तो इ-ई का ‘यू’, ‘उ-ऊ’ का ‘व्’ और ‘ऋ’ का ‘र्’ हो जाता हैं। जैसे-
यण संधि के उदाहरण –
| इ +अ =य | यदि +अपि =यद्यपि |
| इ +आ = या | अति +आवश्यक =अत्यावश्यक |
| इ +उ =यु | अति +उत्तम =अत्युत्तम |
| इ + ऊ = यू | अति +उष्म =अत्यूष्म |
| उ +अ =व | अनु +आय =अन्वय |
| उ +आ =वा | मधु +आलय =मध्वालय |
| मधु +आलय =मध्वालय | गुरु +ओदन= गुवौंदन |
| उ +औ =वौ | गुरु +औदार्य =गुवौंदार्य |
| ऋ+आ =त्रा | पितृ +आदेश=पित्रादेश |
5. अयादि स्वर संधि किसे कहते है
नियम- यदि ‘ए’, ‘ऐ’ ‘ओ’, ‘औ’ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो (क) ‘ए’ का ‘अय्’, (ख ) ‘ऐ’ का ‘आय्’, (ग) ‘ओ’ का ‘अव्’ और (घ) ‘औ’ का ‘आव’ हो जाता है। जैसे-
| (क) ने +अन =नयन चे +अन =चयन शे +अन =शयन श्रो+अन =श्रवन (पद मे ‘र’ होने के कारण ‘न’ का ‘ण’ हो गया) | (ख) नै +अक =नायक गै +अक =गायक |
| (ग) पो +अन =पवन | (घ) श्रौ+अन =श्रावण पौ +अन =पावन पौ +अक =पावक श्रौ+अन =श्रावण (‘श्रावण’ के अनुसार ‘न’ का ‘ण’) |
(II) व्यंजन संधि किसे कहते है
- व्यंजन संधि :- जब दो वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो, तो दोनो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते है। व्यंजन संधि को संस्कृत में “हल संधि” कहते है।
व्यंजन संधि को बनाने के महत्वपूर्ण नियम –
(अ)
(ब)
(स)
(द)
(ई)
(III) विसर्ग संधि किसे कहते है
- विसर्ग संधि :- जब विसर्ग (:) के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते है।
उदाहरण :- पुर: + कार = पुरस्कार
दु: + कर्म = दुष्कर्म
नि: + फल = निष्फल
मन: + योग = मनोयोग
विसर्ग संधि से सम्बंधित प्रमुख नियम उदाहरण सहित –
(अ)
(ब)
(स)
(द)
(ई)
हिंदी व्याकरण और साहित्य से सम्बंधित प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे. – Telegram
